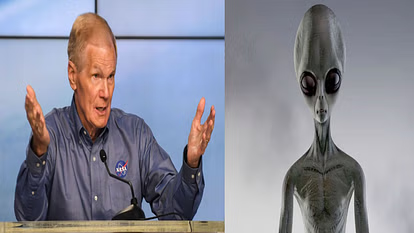उधार के 500/- रुपए से 5 करोड़ रुपए का सफरकहानी श्री कृष्णा पिकल्स की
उधार के 500/- रुपए से 5 करोड़ रुपए बनाना यूं तो आसान काम नहीं होता, लेकिन कृष्णा यादव के कठिनाइयों और संघर्षों से भरे बुलंदशहर से दिल्ली तक के सफर में उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया। आज उनकी कंपनी श्रीकृष्णा पिकल्स 5 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर कर रही है, जो उनके अद्वितीय व्यावसायिक कौशल और मेहनत का प्रमाण है।
बुलंदशहर की कृष्णा यादव का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वह तमाम महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 2001 में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद अचार बनाने के व्यवसाय से उन्होंने अपने उद्यम की शुरुआत की। आज उनकी कंपनी, श्रीकृष्णा पिकल्स, 5 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर कर रही है। यह सफर न केवल संघर्षपूर्ण था, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी है।
प्रारंभिक संघर्ष और प्रेरणा
कृष्णा यादव का जन्म बुलंदशहर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। पारंपरिक ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद, कृष्णा ने हमेशा अपने सपनों को ऊँचा उड़ान दी। उनके परिवार को बुलंदशहर में गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उनके पति की नौकरी चली गई और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ देखते हुए, कृष्णा ने बेहतर अवसर तलाशने का फैसला किया। एक नई शुरुआत की उम्मीद में, वह अपने पति के साथ दिल्ली चली गईं। शादी के बाद, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने काम करने का निश्चय किया। यही वह समय था जब उन्हें फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग का अवसर मिला।
व्यवसाय की शुरुआत
2001 में ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद, कृष्णा ने छोटे पैमाने पर अचार बनाने का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने घर के किचन में ही अचार बनाना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन, और प्रतिस्पर्धा। लेकिन कृष्णा ने हार नहीं मानी। उनके बनाए अचार की गुणवत्ता और स्वाद ने धीरे-धीरे ग्राहकों का दिल जीत लिया।
500 रुपये उधार लेकर शुरू किया काम
दिल्ली में शुरुआती दिनों में कृष्णा को नौकरी खोजने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके सारे प्रयास विफल हो गए। हतोत्साहित न होते हुए, उन्होंने खेती करने का फैसला किया और इसे कुछ वर्षों तक जारी रखा। 2001 में, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में तीन महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस नए ज्ञान के साथ, उन्होंने एक रिश्तेदार से 500 रुपये उधार लिए और दो तरह के अचार बनाने में 3,000 रुपये का निवेश किया।
ऐसे बढ़ता गया भरोसा
अचार के अपने शुरुआती काम से कृष्णा को 5,250 रुपये का मुनाफा हुआ। वैसे तो यह रकम मामूली थी, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था। उन्होंने खुद को अचार के व्यवसाय को बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके पति सड़कों पर उनके बनाए अचार बेचते थे। ग्राहकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने कृष्णा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें उत्पादन बढ़ाने का हौसला मिला।
सफलता की सीढ़ियाँ
कृष्णा की मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे। धीरे-धीरे उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। उनकी कंपनी, श्रीकृष्णा पिकल्स, आज विभिन्न प्रकार के अचार बनाती है जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जो उनके अद्वितीय व्यवसायिक कौशल और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आज करोड़ों की मालकिन
आज, श्रीकृष्णा पिकल्स के बैनर तले, कृष्णा यादव 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों की मालिक हैं। 500 रुपये उधार लेने से लेकर करोड़पति बनने तक की उनकी उद्यमशीलता की यात्रा ने कई महिलाओं को खुद पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया है। महिला उद्यमिता में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कृष्णा को पहचान और सम्मानित किया गया है, जो उन्हें हर जगह इच्छुक उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल बनाता है।
अन्य महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा
कृष्णा यादव की सफलता की कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
अन्य प्रेरणादायक उदाहरण
कृष्णा यादव की तरह ही अन्य महिला उद्यमियों की कहानियाँ भी प्रेरणादायक हैं। जैसे, लिज्जत पापड़ की संस्थापक जसवंतीबेन जमनादास पोपट, जिन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर 1959 में मात्र 80 रुपये की पूंजी से व्यवसाय शुरू किया था और आज लिज्जत पापड़ एक ब्रांड बन चुका है। इसी तरह, सुशीला देवी, जिन्होंने अपने घर के आँगन में सिलाई का काम शुरू किया और आज उनकी सिलाई यूनिट में 100 से अधिक महिलाएँ काम करती हैं।
कृष्णा यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें किसी विशेष संसाधनों या परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस दृढ़ संकल्प, मेहनत, और कभी न हार मानने वाले जज़्बे की। उनके द्वारा स्थापित श्रीकृष्णा पिकल्स की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में किए गए प्रयास निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाते हैं।
कृष्णा यादव की तरह, अगर हम भी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।