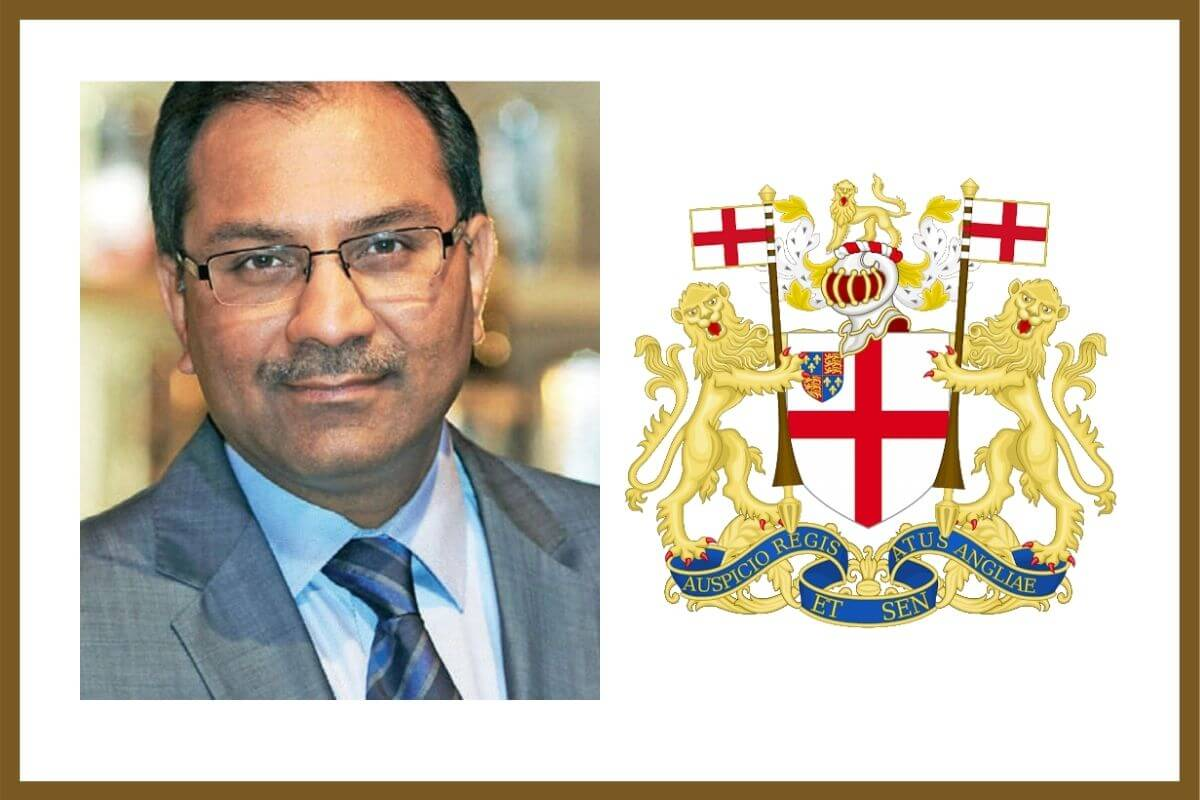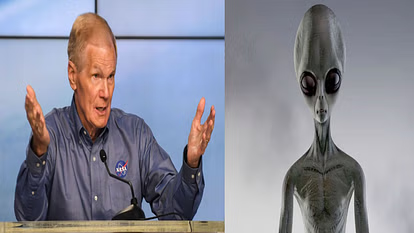पृथ्वी के गहने वृक्षों से ऐसे-ऐसे लाभ जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे आप
वर्षा ऋतु को प्राचीन काल से ही जीवनदायिनी माना गया है, जब समूची धरती हरियाली से ढक जाती है। यह समय केवल कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि वृक्षारोपण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। जब आकाश से अमृत तुल्य जल बरसता है, तो धरती नवजीवन का अनुभव करती है, और इसी नवजीवन में वृक्षारोपण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। वृक्ष, जो धरती की धरोहर हैं, उन्हें इस समय लगाया जाए तो वे न केवल तेजी से बढ़ते हैं, बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जब प्राकृतिक संसाधनों का संकट गहराता जा रहा है, वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है।
वृक्ष केवल छांव और ऑक्सीजन देने तक सीमित नहीं हैं। उनका मूल्य इससे कहीं अधिक है। 1979 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. तारक मोहन दास ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने एक पेड़ की आर्थिक कीमत का आकलन किया। उनके अनुसार, एक पेड़ अपने 50 साल के जीवनकाल में 2 लाख डॉलर की सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में ऑक्सीजन का उत्सर्जन, भूक्षरण रोकने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पानी का पुनर्चक्रण, और हवा को शुद्ध करने जैसी सेवाएं शामिल हैं। आज की महंगाई दर के हिसाब से यह राशि लगभग 5 करोड़ रुपये होती है।
दिल्ली के एनजीओ दिल्ली ग्रीन्स के 2013 के अध्ययन के अनुसार, एक स्वस्थ पेड़ साल भर में जितनी ऑक्सीजन देता है, अगर उसे खरीदा जाए तो उसकी कीमत 30 लाख रुपये से भी अधिक होगी। इस प्रकार, पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक मूल्यवान हैं।
पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों की भूमिका
वृक्षारोपण केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, यह पर्यावरण को संतुलित रखने में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन के अनुसार, देश के उन राज्यों में जहां जंगल कम हो रहे हैं, बाढ़ का खतरा 28% तक बढ़ गया है। वहीं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अध्ययन में भी यही बात सामने आई है कि जिन देशों में प्राकृतिक जंगलों का क्षेत्र 10% तक कम हुआ, वहां बाढ़ की आशंका 4 से 28% तक बढ़ गई।
पेड़ अस्थमा जैसी बीमारियों को रोकने में भी सहायक होते हैं। यूके में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, एक वर्ग किलोमीटर में 343 पेड़ लगाने पर बच्चों में अस्थमा की आशंका 33% तक कम हो जाती है। इसी प्रकार, जंगल बीमारी फैलाने वाले जीवों, खासतौर पर मच्छरों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, 90 के दशक में पेरू में सड़कों के लिए जंगल कटने के कारण मलेरिया के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई।
जैव विविधता और स्वास्थ्य के लिए पेड़ों का महत्व
पेड़ और जंगल जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में पेड़-पौधों की लगभग 50,000 ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। चीन और भारत में सबसे अधिक औषधीय पौधों की किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से 3,000 पौधों का उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। ये पौधे न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि जैव विविधता को बचाने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान नेचर कंजर्वेंसी के एक अध्ययन के अनुसार, शहरों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने से खराब पर्यावरण से होने वाली मौतों को 9% तक कम किया जा सकता है, और हर साल 36,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक पेड़ साल भर में 20 किलोग्राम तक धूल सोखता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और मानव स्वास्थ्य में सुधार होता है।
पेड़: हमारे लिए अनमोल धरोहर
पेड़ हमारे वातावरण का तापमान नियंत्रित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। एक पेड़ साल भर में 22 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है और 100 किलोग्राम तक ऑक्सीजन दे सकता है। इसके अलावा, पेड़ बारिश करवाने और ग्राउंडवाटर बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। एक पेड़ की मदद से सालाना 3500 लीटर पानी बरस सकता है और वह करीब 3700 लीटर पानी को जमीन में पहुंचाने में सहायक होता है।
पेड़ हमारे लिए वायु को फ़िल्टर करके फेफड़ों की रक्षा करते हैं। एक पूर्ण विकसित पेड़ प्रदूषित हवा से 108 किलोग्राम तक छोटे कण और गैसों को अवशोषित कर सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। पेड़ शांति और सुकून प्रदान करते हैं, घर के आसपास सही जगह पेड़ लगाने पर एयर कंडीशनर की जरूरत 30% तक कम हो सकती है, जिससे 20-50% तक बिजली बचाई जा सकती है।
वृक्षों का संरक्षण: एक आवश्यक पहल
आज जब जंगलों की घटती संख्या के कारण पर्यावरणीय असंतुलन गहराता जा रहा है, तो पेड़ों का संरक्षण और अधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। भारत में पिछले 18 सालों में 17,200 करोड़ वर्ग फीट जंगल काटे जा चुके हैं, यानी लगभग 125 करोड़ पेड़। यदि इस गति से पेड़ काटे जाते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भयावह भविष्य की कल्पना की जा सकती है।
पेड़ न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, बल्कि वे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सहायक हैं। इसलिए, हमें वृक्षारोपण के महत्व को समझना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की पहल करनी होगी। यह केवल एक सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रकृति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है।
वृक्षारोपण और संरक्षण की अनिवार्यता
वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण का महत्व और पेड़ों की अमूल्य सेवाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपनी प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। वृक्षारोपण केवल एक सामाजिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी पहल है। हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचने और कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धरती की सौंदर्य और समृद्धि का आनंद ले सकें।
इस वर्षा ऋतु, आइए हम सब मिलकर एक कदम आगे बढ़ाएं और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।